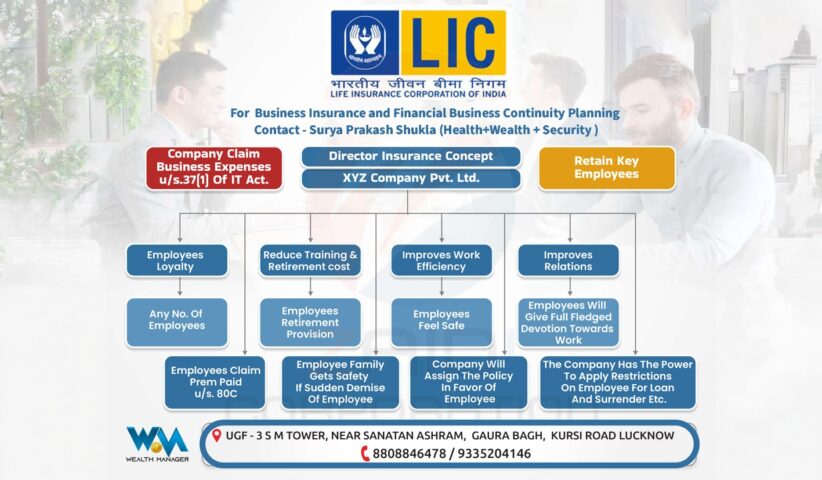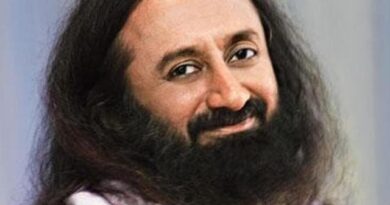विधि विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में शोधार्थी जूही नसीम ने पूर्ण किया गया पीएच.डी. शोध कार्य

बरेली,26 अक्टूबर । विधि विभाग रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली की शोधार्थी जूही नसीम ने प्रो. (डॉ.) गुरमीत सिंह, प्रोफेसर, के.जी.के. कॉलेज, मुरादाबाद के निर्देशन और मार्गदर्शन में अपना शोधकार्य पूर्ण किया है। उनके पीएच.डी. शोध का शीर्षक है —
“Law Relating to Child Labour in India with Special Reference to Hotel Industry in Bareilly District”

यह शोधकार्य भारत में बाल श्रम से संबंधित कानूनों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें विशेष रूप से बरेली जनपद के होटल उद्योग में उनके अनुप्रयोग और प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक, कानूनी, ऐतिहासिक, नियामक, डिजिटल, न्यायिक और प्रायोगिक पहलुओं को समाहित करते हुए यह दर्शाया गया है कि बाल श्रम केवल एक कानूनी उल्लंघन नहीं, बल्कि गरीबी, कमजोर प्रवर्तन तंत्र और डिजिटल युग में उभरते नए शोषण जैसे गहरे सामाजिक-आर्थिक कारणों का परिणाम है। बरेली के होटलों, रेस्टोरेंट, स्पाज, लाउंज, हुक्का बार एवं क्लब आदि में काम करने वाले हजारों असंगठित क्षेत्र के बच्चे जिनको राजू ,बब्लू,छुट्टन, मुन्ना, चिंकी पिंकी, पहाड़ी, नेपाली आदि नामों से बुलाया जाता हैं जिनके पास बहुत कम कानूनी अधिकार होते हैं का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न होता हैं। अत्यधिक काम इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता हैं।
यह शोध सात अध्यायों में बंटा है, जिसमें बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं व संभावित समाधानों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।
यह अध्ययन भारत में बाल श्रम को एक स्थायी सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में पहचानता है, विशेष रूप से होटल उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों में। यह बाल श्रम को भारत की प्रगति पर एक “अमिट कलंक” के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आधुनिकता और पारंपरिक प्रथाओं के साथ-साथ विद्यमान है, जबकि संविधान और कानून इसके उन्मूलन की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।
संवैधानिक उपबंध जैसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 24 (कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध), और बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 भारत की इस दिशा में मंशा को दर्शाते हैं। फिर भी, यह शोध यह रेखांकित करता है कि कानूनी अभिप्राय और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है, जो आर्थिक विषमताओं, ढीले प्रवर्तन और लाभ को नैतिकता पर प्राथमिकता देने से और बढ़ता है।
होटल उद्योग के संदर्भ में, शोध इंगित करता है कि यह क्षेत्र वैश्विक और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (2024 में पर्यटन से भारत के GDP में 10.9% योगदान – विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार), किंतु सस्ते श्रम की मांग भी बढ़ाता है। गरीब परिवारों के बच्चे होटल में झाड़ू-पोंछा, रसोई कार्य, अतिथियों की सेवा, और सामान ढोने जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार छिन जाता है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और यूनिसेफ (UNICEF) की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में लगभग 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं, जिनमें से 5.4 करोड़ खतरनाक कार्यों में लगे हैं।
बरेली जैसे जिले में, जहाँ शहरीकरण और ग्रामीण अविकास का मिश्रण है, अनियमित होटल उद्योग में बाल श्रम फल-फूल रहा है। शोध इस बात पर बल देता है कि कमजोर प्रवर्तन, भ्रष्टाचार, और समाज में बाल श्रम की स्वीकृति इसे “आवश्यक बुराई” के रूप में प्रस्तुत करती है। यद्यपि कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGOs) जागरूकता और पुनर्वास के लिए प्रयासरत हैं, परंतु स्थानीय उद्योगों के प्रतिरोध के कारण उनका प्रभाव सीमित है।
शोध बाल श्रम कानूनों के ऐतिहासिक विकास का भी पता लगाता है, जो पूर्व-औद्योगिक युग से आधुनिक काल तक क्रमिक रूप से विकसित हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्रियों में बाल शोषण के विरुद्ध उठे आंदोलनों ने ब्रिटेन के फैक्ट्री अधिनियमों (1800 के दशक की शुरुआत), यूरोप-अमेरिका के बाल कल्याण आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 1919) और उसके कन्वेंशन – न्यूनतम आयु कन्वेंशन (सं.138) तथा बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सं.182) जैसे मील के पत्थर तय किए।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर, शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो बाल श्रम का उन्मूलन संभव है।
राष्ट्रीय स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 21, 24, 39; बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016; किशोर न्याय अधिनियम, 2015; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) जैसी योजनाएँ उल्लेखनीय हैं।
प्रस्तुत शोध में अमेरिका, यूरोपीय संघ ,कनाडा सहित कई देशों के श्रम कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।
डिजिटल युग में तकनीकी परिवर्तन ने बाल श्रम को नए रूपों में जन्म दिया है। ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदमिक प्रबंधन से सब-कॉन्ट्रैक्टिंग बढ़ी है, जिससे श्रम की पारदर्शिता घटकर शोषण बढ़ा है। आयु सत्यापन की कमी और “एल्गोरिदमिक जटिलता” ने लागत-प्रभावशीलता को मानवाधिकारों पर हावी कर दिया है।
शोध डिजिटल जवाबदेही की मांग करता है — जैसे ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एल्गोरिदम की ऑडिटिंग, और डेटा-साझाकरण तंत्र।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जैसे एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य की जिम्मेदारी को पुनः स्थापित किया है।
बरेली जिले में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि बाल श्रमिकों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं में अधिकारों के प्रति गंभीर जागरूकता की कमी है। अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी स्कूल नहीं गए। नियोक्ता आर्थिक विवशता का हवाला देते हैं, जबकि परिवार गरीबी और अवसरों की कमी को कारण बताते हैं।
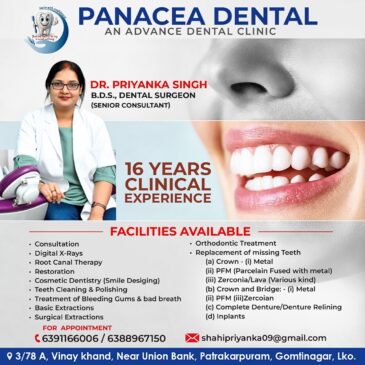
शोध के निम्नलिखित प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:
1) सभी होटल इकाइयों (संगठित-असंगठित) को एक केंद्रीकृत डाटाबेस में लाया जाए, जिससे निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
2) होटल उद्योग में बाल श्रम को खतरनाक व्यवसाय घोषित किया जाए ताकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार पूर्णतः प्रतिबंधित हो सके।
3) आकस्मिक निरीक्षण, प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, डिजिटल उपकरणों द्वारा त्वरित रिपोर्टिंग, और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
4) दंड की राशि को राजस्व से जोड़ा जाए; पुनरावृत्ति करने वालों के लिए कारावास अनिवार्य किया जाए; सार्वजनिक अपराधी सूची (“Naming and Shaming”) जारी की जाए।
5) जिला स्तरीय बहु-एजेंसी टास्क फोर्स गठित की जाए, जो बचाव, पुनर्वास और प्रवर्तन में संयुक्त रूप से कार्य करे।
6) अधिकारियों के लिए पीड़ित-संवेदनशील प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य हो।
7) आयु सत्यापन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
8) निरीक्षण और उल्लंघन की जानकारी ऑनलाइन प्रदर्शित की जाए, ताकि उपभोक्ता नैतिक विकल्प चुन सकें।
9) उच्च जोखिम वाले समुदायों में मीडिया और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
10) बचाए गए बच्चों और स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ और पुनर्संवर्धन कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं।
11) बाल श्रम मुक्त प्रमाणन योजना लागू की जाए, जिसमें CSR फंड से पुनर्वास को समर्थन मिले।
12) बाल श्रम मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं। ————————————————-बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट