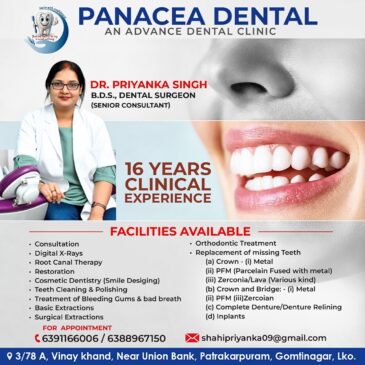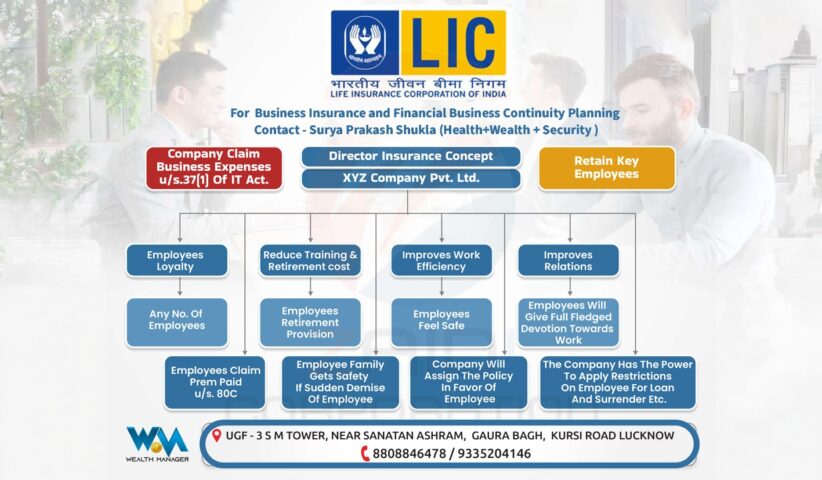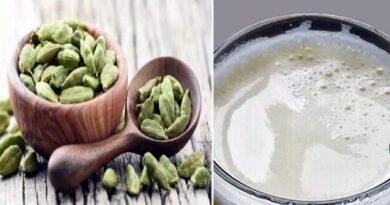सोहराई कला : प्रकृति और संस्कृति का संगम है

लखनऊ, 23 अगस्त 2025, भारत की आदिवासी कलाओं में सोहराई कला एक विशिष्ट और जीवंत परंपरा है, जिसका उद्गम झारखंड, बिहार, ओडिशा और बंगाल के आदिवासी समुदायों में हुआ। यह मात्र सजावटी भित्ति चित्र नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति, कृषि और पशुधन के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। सोहराई नाम उस पर्व से जुड़ा है, जो फसल कटाई और पशुधन पूजा से संबंधित है। सोहराई कला केवल एक चित्रकला परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का संगम है। यह आदिवासी जीवन की आत्मा को प्रकट करती है—जहाँ मिट्टी, पशु, पौधे और मनुष्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आधुनिक दौर में जब प्रकृति और पारिस्थितिकी पर संकट बढ़ रहा है, सोहराई कला हमें सहजीवन और पारिस्थितिक संतुलन का अनूठा संदेश देती है।
लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ए-ब्लॉक राजाजीपुरम में सौंदर्यबोध एवं सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम (2025-26) के अंतर्गत शनिवार को पांच दिवसीय पारंपरिक आदिवासी सोहराई कला कार्यशाला का जीवंत समापन समारोह और छात्र कलाकृतियों की प्रदर्शनी के साथ हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, लखनऊ की सदस्य डॉ. कुमुद सिंह उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्रों के रचनात्मक प्रयासों की प्रशंसा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की पहल युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक चेतना का पोषण करती है और साथ ही स्वदेशी परंपराओं को जीवित रखती है।
प्रधानाचार्या श्रीमती भारती गोसाईं ने छात्रों और शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और कहा कि कलाकृतियों में प्रयुक्त सोहराई कला रूपांकनों और प्राकृतिक रंगों ने कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक गहराई दोनों को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने शैक्षणिक और सांस्कृतिक एवं सौंदर्यबोध शिक्षा को मिलाकर समग्र शिक्षा प्रदान करने के विद्यालय के दृष्टिकोण को दोहराया।
फ्लोरेसेंस आर्ट गैलरी की संस्थापक निदेशक श्रीमती नेहा सिंह ने सोहराई कला से गहराई से जुड़ने के लिए छात्रों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोक विरासत और समकालीन शिक्षा के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करते हैं।
क्यूरेटर एवं कला समीक्षक भूपेंद्र अस्थाना ने छात्रों की कलाकृतियों की विविधता पर प्रकाश डाला, जिसमें पशु-पक्षियों और वृक्षों के पारंपरिक रूपांकनों से लेकर उर्वरता और फसल के प्रतीकों की कल्पनाशील व्याख्याएँ शामिल थीं। सोहराई कला की जड़ें प्राचीन शैलाश्रय चित्रों तक जाती हैं, विशेषकर हज़ारीबाग और सतपहाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रागैतिहासिक गुफा-चित्रकला से। माना जाता है कि इन शैलचित्रों की रूप-भाषा और प्रतीक ही धीरे-धीरे गांवों की मिट्टी की दीवारों पर उतर आए। समय के साथ यह कला स्त्रियों की घरेलू सृजनशीलता बन गई और त्योहारों पर उसका सामुदायिक रूप सामने आया। सोहराई कला की प्रमुख विशेषता इसकी भित्ति चित्रकला तकनीक है। घर की दीवारों को पहले गेरुए या काली मिट्टी से लेपित किया जाता है। उसके ऊपर खड़िया (सफेद), पीली मिट्टी, लाल गेरुआ, काला मैंगनीज़, और हरे रंग के लिए पत्तियों का प्रयोग कर रचना की जाती है। उँगलियाँ, नाख़ून, लकड़ी की टहनियाँ, टूटी कंघी और कपड़े के टुकड़े ही ब्रश का स्थान लेते हैं।
कभी-कभी कंघी-खरोंच तकनीक से नीचे की परत को खुरचकर पैटर्न बनाए जाते हैं। सोहराई कला मुख्यतः फसल और पशुधन पूजा से जुड़ी होती है, जिसमें पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, खेत और प्राकृतिक जीवन के दृश्य अंकित किए जाते हैं। खोवर कला विवाह अवसर पर वधू-कक्ष को सजाने के लिए बनाई जाती है, जिसमें अधिकतर काला-सफेद संयोजन और पैटर्न आधारित आकृतियाँ होती हैं। सोहराई कला स्त्रियों की सामूहिक सृजनशीलता का प्रतीक है। यह न केवल घर को सजाती है, बल्कि समाज के आर्थिक और पारिस्थितिक जीवन को भी दर्शाती है। आज सोहराई कला केवल गाँव की दीवारों तक सीमित नहीं है। इसे कैनवास, कागज़, वस्त्र और शहरी भवनों पर भी चित्रित किया जा रहा है।
इस अवसर पर, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कला विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राजेश कुमार ने कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की और कला संकाय के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की।
श्रीमती पुष्पा देशवाल और श्रीमती सविता विश्वकर्मा द्वारा संचालित कार्यशाला का समापन 50 से अधिक कलाकृतियों के प्रदर्शन के साथ हुआ। समापन सत्र में युवा कलाकारों की रचनात्मक यात्रा का जश्न मनाते हुए भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
समापन समारोह भारत की लोक परंपराओं के संरक्षण और अपने छात्रों की सौंदर्य संवेदनाओं को पोषित करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता का प्रमाण था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सांस्कृतिक जड़ें भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। कार्यक्रम की जीवंतता को और बढ़ाते हुए, प्रतिभागी छात्रों के अभिभावक भी उपस्थित थे। उनकी सक्रिय उपस्थिति और प्रोत्साहन ने बच्चों के सांस्कृतिक विकास में परिवारों को शामिल करने के संस्थान के व्यापक उद्देश्य को प्रतिबिंबित किया। स्कूल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब अभिभावक ऐसी पहलों को देखते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनका सम्मान बढ़ता है।